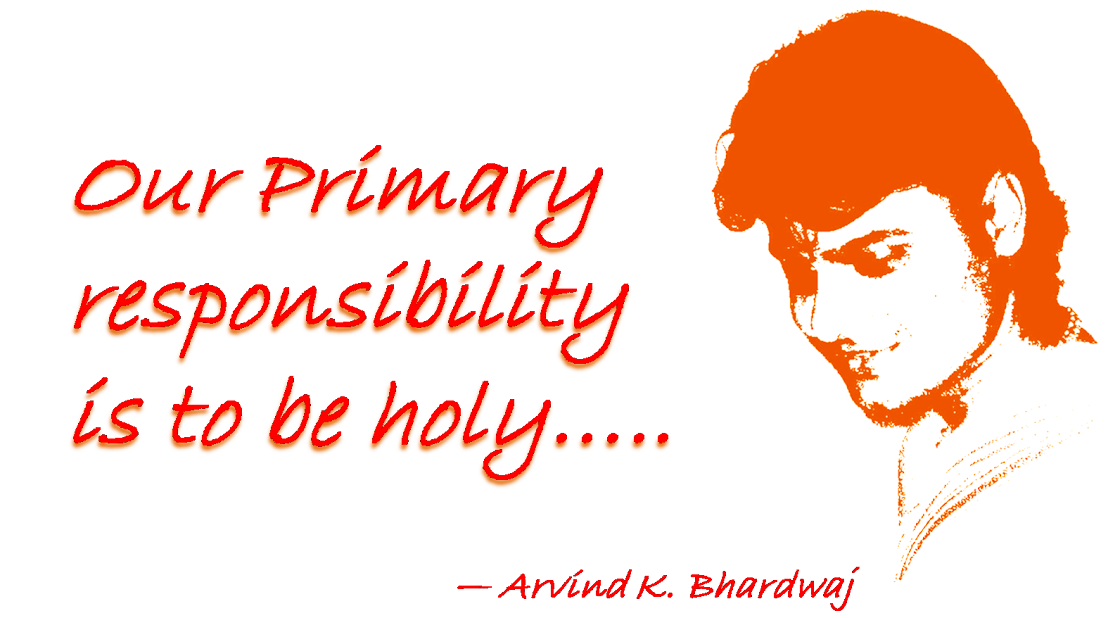"तन्त्र शब्द की दार्शनिक व्याख्या तथा
परिभाषा"
तन्त्र शब्द की निष्पत्ति
प्रसारार्थक ‘तनु’
धातु के साथ त्राणार्थक ‘त्रैङ’ धातु के संयोग से होती है । तन्त्र शब्द की दार्शनिक
व्याख्या साङ्ख्य के परिणामवाद के आधार पर की जाती है तथा तन्त्र की यह व्याख्या
ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है जो तन्त्र के मूल, उद्देश्य तथा मर्म का निर्मल निरूपण करती है
और साथ ही साथ तन्त्र के तात्त्विकानुसंधान के मार्ग को प्रशस्त करती है ।
साङ्ख्य दर्शन में सत्कार्यवाद अथवा
कारणवाद को ही परिणामवाद के नाम से जाना जाता है । “परिणामे तु रूपान्तरं
तिरोभवति । रूपान्तरं च प्रादुर्भवति ॥” (ई० प्रत्यभिज्ञाविवृति वि०अ० १ वि०)
अर्थात् किसी पदार्थ के एक रूप का तिरोभाव होकर दूसरे रूप का प्रकट होना ही ‘परिणाम’ कहलाता है । जैसे – तिल से तैल का निकलना ।
साङ्ख्य के परिणामवाद में यह स्पष्ट किया
गया है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त
रूप से विद्यमान रहता है । कार्य की अव्यक्तावस्था ही ‘कारण’ है तथा कारण की व्यक्तावस्था ही ‘कार्य’ कहलाती है । कारण सत् है तो कार्य
भी सत् ही है – यही सत्कार्यवाद है । कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है – यही कारणवाद
है । कारण का परिणाम कार्य है – यही परिणामवाद है । उदाहरणतः दही से घी का बनना ।
यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि उपादान कारण दही से सर्वथा
विलक्षण कार्य घी की उत्पत्ति हो रही है । साङ्ख्य के इस सिद्धान्त का वेदान्त भी
समर्थन करता है । “दृश्यते तु” (ब्रह्मसूत्र २.१.६) श्रुति में
उपादान कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का उल्लेख देखा जाता है । इस सूत्र
को दृढ़ता के साथ सिद्ध करने के लिए — “यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः
सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥” (मु०उ० १.१.७) अर्थात् जिस प्रकार
मकड़ी जाले को बनाती है और निगल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वी में अनेक प्रकार की
औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार मनुष्य से बाल और रोएँ
उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह विश्व उत्पन्न होता है । — इस श्रुति के द्वारा यह भी समझाया
गया है कि उपादानकारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति सम्भव है । कारण से कार्य की
उत्पत्ति होती है, जब तक कार्य प्रकट नहीं होता तब तक कारण की सत्ता का भी भान नहीं होता है
। वैसे तो कारण सदैव सूक्ष्मावस्था में वर्तमान रहता है परन्तु जब तक कारण कार्यरूप
में परिणत नहीं होता तब तक कारण के अभाव की मिथ्या प्रतीति होती है । वस्तुतः कारण
का अभाव नहीं है, वह तो सूक्ष्मरूप में विद्यमान है । “सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिर्नाभावात्
कार्यतस्तदुपलब्धेः।” (साङ्ख्यकारिका-८) अर्थात् यदि कोई वस्तु दिखाई न
दे तो उसका कारण सूक्ष्मता है, अभाव नहीं, क्योकिं उससे उत्पन्न होने वाला कार्य उसकी सत्ता को प्रकाशित करता है ।
तैत्तिरीयोपनिषद् की श्रुति कहती है
कि - “असद् वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुरुत ।
तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते ।” (तै०उ० २.७) अर्थात् यह सब पहले असत् ही था, उसी से सत् उत्पन्न
हुआ; उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में बनाया, इसलिये उसे सुकृत कहते हैं । इस श्रुति में ‘ प्रकट होने से पहले
जो अप्रकट रूप में रहना धर्मान्तर है, इसी को असत् नाम से
कहा गया है । छान्दोग्योपनिषद् में इस तथ्य को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है – “तद्धैक
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ।“ (छा०उ० ६.२.१)
अर्थात् कोई कहते हैं कि पहले यह जगत् असत् ही था,
अकेला वही अद्वितीय था, फिर उस असत् से सत् उत्पन्न हुआ । यह बतलाकर श्रुति स्वयं ही निवारण करती है – “कुतस्तु खलु सोम्यैवं
स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति ।”
(छा०उ० ६.२.२) अर्थात् हे सोम्य ! ऐसा होना कैसे सम्भव है, असत् से सत् कैसे उत्पन्न हो सकता है ? कहने का अर्थ यह है कि अभावसे भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । “सत्त्वेव
सोम्येदमग्र आसीत् ।” (छा०उ० ६.२.२) अर्थात् हे सोम्य ! यह सब पहले सत् ही था ।
तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति से पहले यह जगत्
अप्रकट (असत्) था, फिर उससे सत् की उत्पत्ति हुई
अर्थात् अप्रकट से प्रकट हो गया । ‘यह सब पहले सत् ही था’ – ऐसा श्रुति ने निश्चय किया है । अतः यहाँ
सत्कार्यवाद की ही सिद्धि होती है ।
वेदान्त का विवर्तवाद भी ‘तन्त्र के दार्शनिक
दृष्टिकोण’ को समझने में उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना साङ्ख्य
का परिणामवाद । “विवर्तो हि असत्यरूप निर्भासम ।” (अभिनवगुप्त :
ई०प्र०वि०वि०) अर्थात् किसी पदार्थ का असत्यरूप में निर्भास होना ‘विवर्त’ है । जैसे – रस्सी
में सर्पाभास होना । एक ही पृथिवी तत्त्व के अनेक प्रकार के कार्य घट, सूत, काष्ठ आदि में परस्पर भेद की प्रतीति अविद्या
के कारण होती है । जिस प्रकार घट मिट्टी का कार्य है उसी प्रकार सूत व काष्ठ भी
मिट्टी के ही कार्य हैं, इनका प्रादुर्भाव मिट्टी से होता है
तथा इनका तिरोभाव मिट्टी में ही हो जाता है । इनमें दृष्टिगत होने वाला नाम तथा
रूप भेद मिथ्या है । “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः” (ब्रह्मसूत्र
२.१.१४) अर्थात् आरम्भण शब्द आदि हेतुओं से कार्य की कारण से अनन्यता सिद्ध होती
है । “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।” (छा०उ०
६.१.४) अर्थात् हे सोम्य! जिस प्रकार
मिट्टी के एक ढेले का तत्त्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले सभी कार्य
जाने हुए हो जाते हैं, उनके नाम और रूप के भेद तो व्यवहार के लिए हैं,
वाणी से उनका कथन (मिथ्या) मात्र होता है, वास्तव में वह
कार्य रूप घट आदि होते हुए भी वह कारण रूप मिट्टी ही हैं ।
परिणामवाद उपादान कारण से विलक्षण
कार्य की उत्पत्ति सिद्ध करता है तो विवर्तवाद कार्य में रहने वाले कारण से
विलक्षण नाम और रूप के भेद को मिथ्या सिद्ध करता है । प्राचीन विद्वानों ने
विवर्तवाद और परिणामवाद को पर्याय के रूप में स्वीकार किया था परन्तु परवर्ती
विद्वनों द्वारा इन्हें अलग-अलग माना जाने लगा । परिणामवाद और विवर्तवाद यह दोनों
सम्मिलितावस्था में ही तन्त्र के वास्तविक रूप को निरूपित कर सकते हैं क्योंकि
तन्त्र का दार्शनिक सिद्धान्त इन दोनों को पर्याय के रूप में ग्रहण करता है ।
आधुनिक दर्शनशास्त्र के अनुसार भी परिणामवाद और विवर्तवाद में कोई गम्भीर मतभेद
दृष्टिगोचर नहीं होता । वेदान्त में परिणामवाद के सिद्धान्त का पोषण किया गया है
क्योंकि यही व्यक्ति को विवर्तवाद के केन्द्रीय सिद्धान्त तक ले जाता है । परिणामवाद
को आधार बनाकर तन्त्र की ओर अग्रसर होने का मार्ग इसलिए अङ्गीकृत किया गया क्योंकि
यह सगुण ब्रह्म के ध्यान के लिए उपयोगी है ।
तान्त्रिकों का मत है कि इस जगत् का
कारण ब्रह्म है जो शिव नाम से जाना जाता है (तन्त्र में जगत् के कारण ‘ब्रह्म’ की ‘शिव’ संज्ञा है) तथा यह
सम्पूर्ण सृष्टि (प्रपञ्च) उस ब्रह्म अर्थात् शिव का कार्य है । ‘कारण की कार्य रूप में अभिव्यक्ति ‘कारण का व्यापार’ है, कारण
का यह व्यापार ही शक्ति है’ अथवा ‘कारण
जिस सामर्थ्य द्वारा कार्य में परिणत होता है, वह कारण की
शक्ति कहलाती है’ । सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म
अर्थात् शिव का अपनी सामर्थ्य अर्थात् शक्तिके द्वारा सृष्टि अर्थात् प्रपञ्च के
रूप में प्रसार हो जाता है । इस प्रपञ्च की स्थिति भी शक्तिके द्वारा रहती है तथा
इस शक्ति के द्वारा ही प्रपञ्च का शिव में लय हो जाता है अर्थात् कार्य का कारण
में लय हो जाता है । इस प्रकार शक्ति द्वारा सृष्टि, स्थिति
तथा लय का चक्रियक्रम सम्पन्न होता रहता है । यह समस्त जगत् प्रकट होने से पहले भी
‘शिव की शक्ति’ के रूप में अवश्य था ।
इसका वर्तमान स्वरूप उसी प्रकार अप्रकट था जिस प्रकार स्वर्ण के विकार आभूषणादि
उत्पत्ति के पहले और लय होने के पश्चात् अपने कारण रूप स्वर्ण में शक्तिरूप से
रहते हैं । शक्ति, शक्तिमान् (शिव) में अभेद होने के कारण
उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता, उसी प्रकार
यह जड-चेतनात्मक अखिल विश्व उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद शिव मे शक्तिरूप से
अव्यक्त रहता है । अतः जगत् की शिव से अनन्यता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती ।
अतः यह अखिल प्रपञ्च ‘शक्ति की लीला’
है । जिसे वेदान्त में ‘माया’ के नाम
से जाना जाता है । माया की उपाधि से युक्त होने पर ब्रह्म निर्गुण नहीं रह जाता, वह सगुण हो जाता है । माया की उपाधि से युक्त ब्रह्म (शिव-शक्ति युगल) ही
संसार का कर्ता है । यह जगत् शिव का विवर्त है और शक्ति का परिणाम ।
समस्त आन्तरिक तथा बाह्य जगत्प्रपञ्च
मूलप्रकृति रूपी पराशक्ति का विकार – विस्तार है । पराशक्ति का विकार – विस्तार
असीमित है । पराशक्ति का रूप अक्षरात्मक है । अखिल प्रपञ्च का प्रादुर्भाव वर्णमयी
पराशक्ति के ‘हकार’ से होता है और अन्ततः उसी में सकल प्रपञ्च का
तिरोभाव हो जाता है । पराशक्ति मनुष्य शरीर के मूलाधार चक्र में परावाक् कुण्डलिनी
के रूप में प्रसुप्त रहती है । यह परावाक् स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा से
त्रि-चतुः-पञ्च-षट्-सप्त-अष्ट-दश-द्वादश-पञ्चाशत् गुणित होकर अपना आत्मविस्तार
करती है । जब यह कुण्डलिनी पञ्चाशत् गुणित होती है तब यह मूलाधार में अपने
अधिष्ठानरूप पुरूष तत्त्व से दिव्यभाव प्राप्त कर नाद के साथ सुषुम्ना के मार्ग से
कण्ठादि स्थानों का स्पर्श करती हुई अ से क्ष तक के पचास वर्णों के रूप में
अभिव्यक्त होती है । समस्त जगत् की सृष्टि अक्षर अर्थात् पराशक्ति शब्दब्रह्म ‘परावाक्’ से हुई है । यहाँ तन्त्र शब्द की
प्रसारार्थक ‘तनु’ धातु का – ‘पराशक्ति का आत्मविस्तार’ यह अर्थ प्रकट होता है ।
विस्तार होने से उद्भूत विस्तृत वस्तु की रक्षा अत्यन्तावश्यक है । यदि इस विस्तृत
प्रपञ्च की रक्षा न की जाये तो इस जगत्प्रपञ्च का तत्काल ही नाश हो जायेगा और
शक्ति की लीला शान्त हो जायेगी । अतः अपनी लीला को सतत् रखनेके लिये पराशक्ति अपने
आत्मविस्तार का त्राण करती है – यही तन्त्र शब्द की त्राणार्थक ‘त्रैङ’ धातु का अर्थ है । ‘पराशक्ति के तनन द्वारा अभिव्यक्त प्रपञ्च तथा पराशक्ति द्वारा इस प्रपञ्च
का त्राण ’ – यही है तन्त्र का अर्थ । सरल शब्दों में यह कहा
जा सकता है कि पराशक्ति द्वारा रक्षित यह सकल प्रपञ्च अर्थात् सृष्टि ही तन्त्र है,
जो शिव का विवर्त तथा शक्ति का परिणाम है ।
—
अरविन्द कुमार भारद्वाज
१६-०५-२०१६